क्या है दुनिया के ऊर्जा संकट का समाधान ?
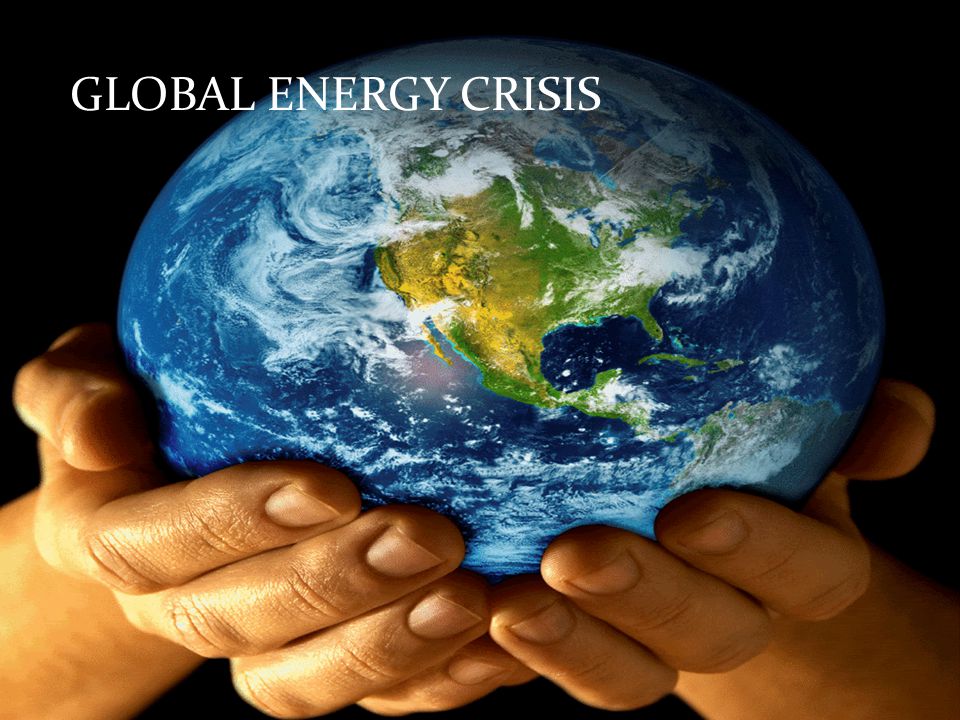
सूर्य की चमक इंसानों के लिए हज़ारों साल से आश्चर्य की वजह रही है.
लेकिन करीब सौ साल पहले खोज हुई कि सूर्य की बेशुमार ऊर्जा का कारण है न्यूक्लियर रिएक्शन, जिसे फ्यूज़न कहा जाता है.
अगर धरती पर उसी तरह का फ्यूज़न कराया जा सके तो बहुत कुछ बदल सकता है. दुनिया भर के लोगों को बेशुमार ऊर्जा मिल सकती है.
बीते करीब सौ साल से फ्यूज़न कराने की कोशिश जारी है. करीब पचास साल से दावे किए जा रहे हैं कि ये लक्ष्य अगले कुछ दशक में हासिल हो जाएगा. इस साल फरवरी में इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने दावा किया कि वो पांच सेकेंड तक ऐसा करने में कामयाब हुए हैं.
अब सवाल है कि क्या न्यूक्लियर फ्यूज़न से दुनिया को ऊर्जा संकट का स्थायी समाधान मिल सकता है?
फ्यूजन में यही होता है. हम परमाणुओं को लेते हैं. उन्हें एक साथ जोड़ते हैं और इस प्रक्रिया में द्रव्यमान घट जाता है और अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है.
ये सीधी सी प्रक्रिया मालूम होती है तो फिर हमने इसे काफी पहले ही क्यों नहीं आजमाया? वजह है इस प्रक्रिया से जुड़ी दिक्कतें.
परमाणु हमारी दुनिया का सबसे छोटा हिस्सा हैं. वो एक दूसरे से जुड़कर मॉलिक्यूल यानी अणु बनाते हैं. मसलन हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलकर पानी का एक अणु बनाते हैं. ये एक अणु तीन परमाणु से मिलकर बनता है.
लेकिन फ्यूज़न में आप दो परमाणु लेते हैं और वहां आपको एक अणु नहीं बनाना है बल्कि आप दोनों को मिलाकर एक परमाणु बना रहे होते हैं. बहुत ताकत के साथ पास लाने पर वो जुड़ जाते हैं.
ये संपर्क बहुत ज़ोरदार होता है. दूरी बहुत ही कम होती है. अगर आप दो प्रोटोन को एक दूसरे के बेहद करीब ले आते हैं तो एक दूसरे को खींचने वाला परमाणविक बल एक दूसरे को परे धकेलने वाले विद्युतीय बल से ज़्यादा होता है और वो आपस में जुड़ जाते हैं.
और जब ऐसा होता है तो बड़ी मात्रा में ऊर्जा बाहर आती है. इसके पीछे का कारण एक चर्चित फॉर्मूले से समझा जा सकता है. ‘ई ईक्वल्स एमसी स्क्वैयर’ (E =mc2).
साल 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये समीकरण सामने रखा और समझाया कि तारों और परमाणु विस्फोटों में ऊर्जा कैसे बाहर आती है.
ये समीकरण बताता है कि परमाणु के वजन में हुई कमी ऊर्जा में तब्दील हो जाती है.
मौजूदा न्यूक्लियर पावर प्लांट इस तरह से यानी परमाणुओं को जोड़कर ऊर्जा हासिल नहीं करते हैं. वो परमाणुओं को अलग अलग करते हैं.
परमाणुओं को अलग करने की प्रक्रिया फिज़न यानी विखंडन कहलाती है. इसमें भी द्रव्यमान में कमी आती है और आइंस्टीन का फॉर्मूला यहां भी लागू होता है.
तारे की ताक़त
साल 1920 में ब्रिटेन के एस्ट्रोफिजिसिस्ट आर्थर एडिंगटन ने कार्डिफ़ में करीब हज़ार वैज्ञानिकों के सामने एक भाषण दिया. आर्थर एडिंगटन ने वहां जुटे वैज्ञानिकों को बिल्कुल नई बात बताई. उन्होंने दावा किया कि सूर्य की ऊर्जा की वजह है फ्यूज़न.
प्रिंसटन प्लाज़्मा फिजिक्स लैबोरेट्री से जुड़ीं और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल रिसर्चर फातिमा इब्राहिमी के मुताबिक, ” उन्होंने बताया कि तारों में हल्के परमाणुओं का आपस में संपर्क होता है. फ्यूज़न रिएक्शन के जरिए बहुत सारी ऊर्जा पैदा की जा सकती है. 1920 के दशक के शुरुआती सालों में ये बात सामने आई कि तारे अपनी ऊर्जा कैसे पैदा करते हैं.”
आर्थर एडिंगटन ने बताया कि सूर्य के अंदर हाइड्रोजन परमाणु इस रफ़्तार से टकराते हैं कि वो आपस में जुड़कर एक नए तत्व हीलियम के परमाणु बना देते हैं.
इस प्रक्रिया में क्षय होने वाला द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाता है. करीब एक दशक बाद ब्रिटेन के वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सूर्य के अंदर होने वाले रिएक्शन को एक प्रयोगशाला में आजमाया. उन्होंने इसके लिए हाइड्रोजन के दो अलग किस्म के परमाणुओं ट्रिटियम और ड्यूटेरियम का इस्तेमाल किया.
5 करोड़ डिग्री तापमान
फ्रांस के दक्षिण में दुनिया का पहला न्यूक्लियर फ्यूज़न पावर स्टेशन बनाने की परियोजना पर काम जारी है. इसे नाम दिया गया है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर. तीस से ज़्यादा देश अब तक इसमें करीब 20 अरब यूरो लगा चुके हैं.
सेंटर फॉर डॉक्टोरल ट्रेनिंग इन न्यूक्लियर एनर्जी फ्यूचर्स के डायरेक्टर मार्क वेनमैन कहते हैं, ” ये एक बहुत बड़ी परियोजना है. दुनिया की सभी प्रमुख शक्तियों ने इसमें निवेश किया है. ये पहली परियोजना है जिसके रिएक्टर से साबित होगा कि न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए आप जितनी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा हासिल करते हैं. उम्मीद की जा रही है कि बाहर निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा 10 गुना होगी.”
ये बहुत ही जटिल प्रोजेक्ट है. इसमें लाखों पुरजे लगे हैं. ये टोकोमाक डिज़ाइन पर आधारित है.
मार्क बताते हैं कि प्लाज़्मा वैक्यूम वेसल में रहता है. उसका आकार डोनट की तरह होता है. इसके चारों और खास प्रक्रिया से ठंडी की गई बहुत बड़ी चुंबक होती है.
हाइड्रोजन प्लाज़्मा को पांच करोड़ डिग्री सेंटिग्रेड के तापमान पर रखे जाने की ज़रूरत होती है. ये सूर्य के तापमान का दस गुना है.
मार्क बताते हैं कि गर्म किए जाने पर गैस और जेली जैसी चीज़ सामने होती है. वहां कोई परमाणु नहीं होते. वहां पॉज़िटिव चार्ज वाला केंद्र होता है और नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं. ये सूप जैसा होता है जो डोनट के आकार में बहने लगता है. हाइड्रोजन परमाणु टकराते हैं और हीलियम बनाते हैं. रिएक्शन जारी रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि वो बाहर निकल सकें.
मार्क वेनमैन बताते हैं, ” इसके तले में डाइवर्टर होता है. ये आपकी कार के एग्ज़ास्टर की तरह होता है. मान लीजिए आप अपनी कार में जिस तरह ईंधन जलाते हैं, उसी तरह यहां प्लाज़्मा जलाया जाए तो कुछ बाई प्रोडक्ट सामने आते हैं. इनमें से एक होता है हीलियम परमाणु. हमें उन्हें बाहर निकालना होगा. नहीं तो वो प्लाज़्मा को दूषित करते हुए पूरी प्रक्रिया को रोक देंगे.”
सामग्री से जुड़ी चुनौती
शेफ़ील्ड यूनिवर्सिटी की सीनियर लेक्चरर डॉ. एमी गैंडी कहती हैं, ” मुझे लगता है कि फ्यूजन तकनीक और फ्यूजन ऊर्जा के जरिए दुनिया को अच्छी मात्रा में एनर्जी उपलब्ध कराई जा सकती है. वो भी बिना कार्बन डाईऑक्साइड और न्यूक्लियर रेडियोएक्टिव कचरा पैदा किए हुए. अपने ग्रह को बचाने की दिशा में ये गेमचेंजर साबित हो सकता है.”
वो बताती हैं कि उनका विभाग ऐसी सामग्री विकसित करने के लिए काम कर रहा है जिसकी मदद से न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर अंदर का भारी ताप सह सके और लंबे वक्त तक काम कर सके.
डॉ. एमी गैंडी कहती हैं, ” हम कोशिश कर रहे हैं कि सामग्री उन स्थितियों में लंबे समय तक टिके ताकि आप फ्यूजन डिवाइस में एक किस्म की सामग्री डालें और वो डिवाइस ताउम्र ऑपरेट हो सके. ताउम्र सामग्री बदलने जैसी लागत न बढ़ानी पड़े.”
रिएक्टर में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन के जिन प्रकारों को इस्तेमाल किया जाता है, उनमें से एक ट्रिटियम है. इसकी उपलब्धता कम है.
लेकिन फ्यूज़न रिएक्टर में एक और तरह की हाइड्रोजन इस्तेमाल होती है. ये है ड्यूटेरियम. इसे लेकर अच्छी खबर है.
डॉ. एमी गैंडी बताती हैं, ” ड्यूटेरियम आसानी से उपलब्ध है. समुद्र के पानी से ड्यूटेरियम निकालने की तकनीक पर हम पहले से ही काम कर रहे हैं. वैज्ञानिक और इंजीनियर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. मेडिकल डिवाइस में भी ये इस्तेमाल होती है. इसकी प्रक्रिया जानी पहचानी है.”
लेकिन फ्यूज़न कराना मुश्किल है. ब्रिटेन में फ्यूज़न रिएक्टर सिर्फ पांच सेकेंड तक ही चल सका. लेकिन एमी बताती हैं कि फ्रांस के रिएक्टर के डिज़ाइन में अहम सुधार किया गया है.
डॉ. एमी गैंडी कहती हैं, ” पांच सेकेंड ही चल पाने का कारण ये है कि वो साधारण तांबे से बनी चुंबक इस्तेमाल कर रहे थे. ये पांच सेकेंड बाद बहुत ज़्यादा गर्म हो गई. भविष्य की फ्यूज़न डिवाइस में सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट का इस्तेमाल होगा. ये चुबंकीय शक्ति में इजाफा कर देती है और तीन सौ से लेकर पांच सौ सेकेंड तक फ्यूज़न हो सकता है.”





